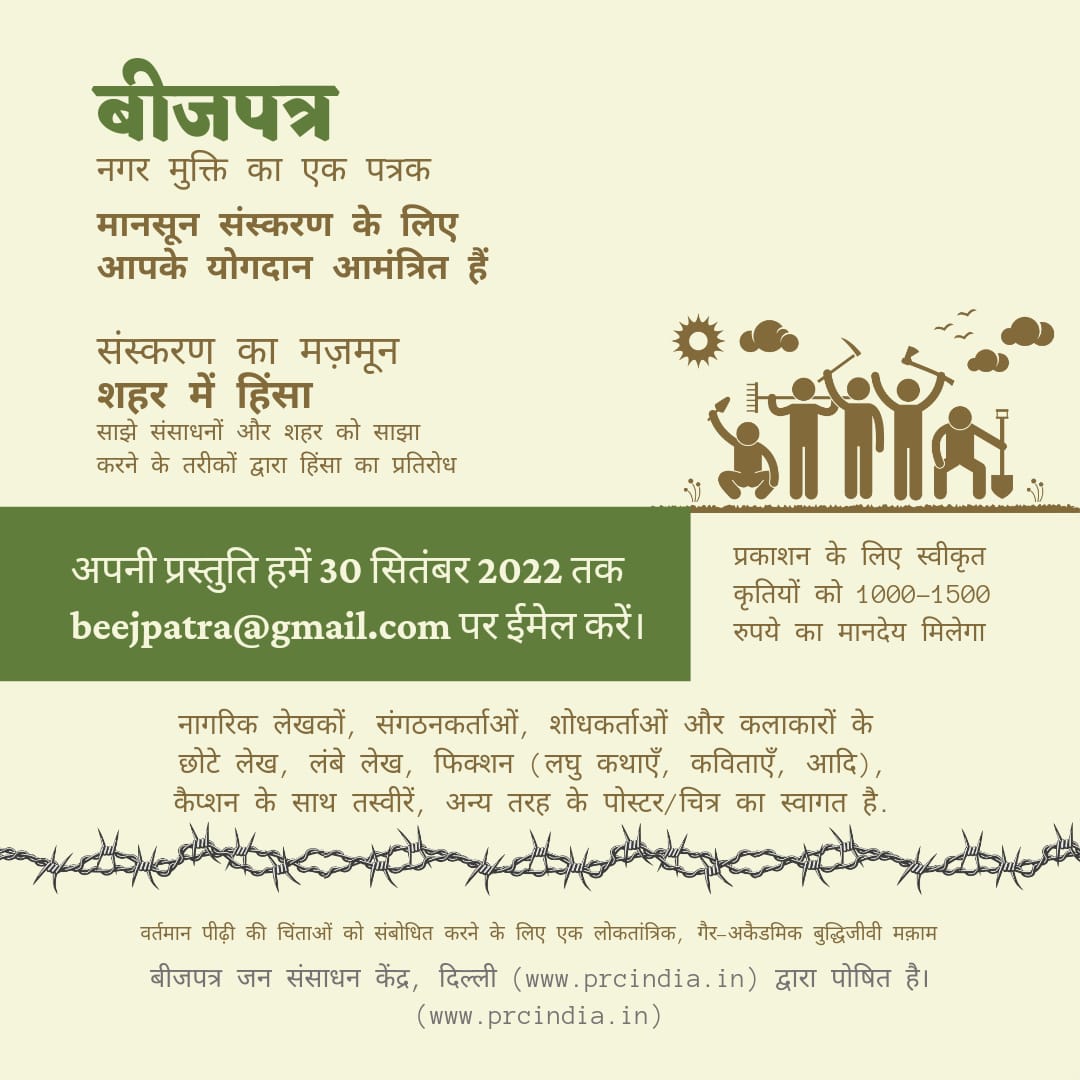बीजपत्र: नगर मुक्ति का एक पत्रक
पत्रक के बारे में
“बीजपत्र” बीज का वह भाग होता है जो बीज में जड़ उगने तक बीज को पोषण देता है। इस पत्रक की शुरुआत एक त्रैमासिक के रूप में शहरी खेती की मौजूदा स्थिति और उससे जुड़ी संभावनाओं पर नयी समझ बनाने और उसे साझा करने के लिए की गयी थी। पिछले दो सालों में हमने इस पत्रक के छह संस्करण प्रकाशित किये जिनमें कुल 45 लेख छप। इसके जरिये शहरी खेती में रुचि रखने वाले एक बड़े समूह को हम एक साथ ला पाए। बहुत कम समय में ही बीजपत्र शहरी मुद्दों, विकल्पों, साझे संसाधनों (कॉमन्स) और रोज़मर्रा के आम मसलों पर जमीनी ज्ञान और अनुभव पेश करने का एक नायाब साधन बन गया।
इस दौरान बढ़ी सांप्रदायिकता, फासीवाद और पर्यावरण संकट की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सम्पादन टीम ने बीजपत्र की समकालिकता, दायरे और उद्देश्य पर दोबारा गौर किया। विस्तार से चर्चा के बाद, हमने शहरों में सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक बदलाव लाने और बुनियादी बदलाव पर विमर्श में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को बीजपत्र से जोड़ने का फैसला लिया। इस तरह, अब बीजपत्र भारतीय सरहद के अन्दर स्थित शहरों और शहरों में आधारित सामाजिक आंदोलनों के लिए मुक्तिवादी विचारों की जड़ को विकसित करेगा लेकिन ऐसा करने में हम दुनिया के अन्य हिस्सों में शहरों में हो रहे बदलावों से संवाद बनाकर रखेंगे। बीजपत्र के मूल में ये ख़याल है कि आज प्रतिरोध के कार्यक्रमों की ये जिम्मेदारी है कि वे जाति, वर्ग, जेंडर, मजहब, उम्र और शारीरिक क्षमता आदि पर आधारित ऊँच-नीच को पनपने से रोकें ताकि इन सभी में एक पारस्परिक सम्बन्ध को देखते हुए हम वर्तमान में ही एक वैकल्पिक भविष्य रच सकें।
हम प्रतिबद्ध हैं कि इस पत्रक को एक नायाब, लोकतांत्रिक, गैर-अकैडमिक बौद्धिक जगह बना सकें जहाँ नई पीढ़ी की चिंताओं को संबोधित किया जाता हो। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो सत्ता से निराश हो चुके लोगों को आपस में जोड़े – उन लोगों को जो एक बार फिर से शहर को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं, जहां प्रकृति के साथ संतुलन में एक ख़ुशहाल, सामूहिक जीवन बिताया जा सके।
इसी भावना के साथ, हम नागरिक लेखकों, संगठनकर्ताओं, शोधकर्ताओं, और कलाकारों के ऐसे छोटे लेख, लम्बे लेख, फिक्शन (लघु कथाएं, कवितायें, आदि), कैप्शन के साथ तस्वीरें, अन्य तरह के पोस्टर/ चित्र आमंत्रित करते हैं जो बढ़ते अंधेर पर सवाल उठायें और आगे के रास्ते पर रोशनी डालें। हम खास तौर पर युवा और नए लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमसे जुड़ें और बताएं कि वे कैसे इस पत्रक में योगदान करना चाहते हैं, ताकि हम शुरुआत से ही उन्हें उनके योगदान में मदद कर सकें। हम ऐसे योगदान ही स्वीकार कर पायेंगे जो अभी तक किसी भी रूप में (प्रिंट या ऑनलाइन) कहीं और प्रकाशित नहीं हुए हैं। हालाँकि, बीजपत्र एक “कॉपीलेफ्ट” प्रकाशन है, और इसलिए जो लेख हम प्रकाशित करते हैं, उन्हें उनके लेखक (या लेखक से अनुमति लेकर अन्य कोई) कहीं और फिर से प्रकाशित कर सकते हैं। हमसे बातचीत की शुरुआत करने के लिए आप हमें beejpatra@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कॉन्सेप्ट नोट: बीजपत्र मानसून संस्करण, वर्ष-2022 के लिए आपके योगदान आमंत्रित हैं
एक जटिल व्यवस्था के जरिये लोगों, स्थानों, संस्थानों और प्रकृति से मिलकर एक शहर बनता है। लेकिन शहरों में विकास का जो मॉडल अपनाया जा रहा है, वह बिना सोचे-समझे संसाधनों के इस्तेमाल और शहरों के अनंत फैलाव की मानसिकता पर आधारित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कुछ ख़ास लोगों की संपत्ति और शक्ति को बढ़ाना है। इस मॉडल से जिन वर्गों को लाभ होता है, उन्हें शहरी जीवन के जटिल संबंधों की कोई परवाह नहीं बल्कि हाशिए के समुदायों के हक़ को हथियाकर तरक्की करना ही उनकी फितरत है।
हिंसा इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंसा कई रूपों में सामाजिक जीवन के सभी हिस्सों में हावी है, जैसे पितृसत्तात्मक पूंजीवाद की हिंसा, समुदायों के खिलाफ और प्रकृति के खिलाफ राज्य द्वारा हिंसा। नगरों के इतिहास को पढ़कर ऐसा लग सकता है कि शहर के साथ साथ ही सभ्यता का भी विकास हुआ है। लेकिन शहरों में ही, शहर के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार कई महत्वपूर्ण कारक ख़तम होते हुए भी दिखते हैं। आज के समय में हिंसा और शहरी जीवन एक-दूसरे में इतने गुंथे हुए दिखाई देते हैं कि यह सोचना भी मुश्किल है कि क्या कोई अहिंसक शहर कभी था या कभी हो सकता है।
इसलिए, नए बीजपत्र का पहला संस्करण शहर में हिंसा और दमन के अलग-अलग रूपों और उनके खिलाफ उठती नागरिक आवाज़ों पर केन्द्रित रहेगा। हम जानते हैं कि बीजपत्र जैसे जर्नल के एक संस्करण में समेटने के लिए यह काफी व्यापक विषय है। पर ये बात भी है कि शहर को सामाजिक और पर्यावरणीय अन्यायों से मुक्त करने का हमारा संकल्प इस विषय पर समझ बेहतर किये बिना कभी पूरा नहीं होगा। आज ज़्यादातर समाज राज्य (स्टेट) और कॉर्पोरेट शक्तियों के ऊपर आँख मूंदकर कर भरोसा कर ले रहा है और अपने सामाजिक भविष्य में अपनी नाम मात्र की हिस्सेदारी से ही संतुष्ट है। अन्याय से लड़ने और शहर पर वाजिब हिस्सेदारी कायम करने के हमारे इस साझा संकल्प का संभ्रांत वर्ग के इरादों से सीधा टकराव है। इसलिए उन राजनीतिक संस्थानों पर से भी धीरे-धीरे लोगों का भरोसा उठ रहा है जो अब सिर्फ कहने के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित रह गए हैं। शहरी समाज के इस प्रकार प्रकृति-विरोधी होते जाने और खण्डित होने के खिलाफ संगठित होने की जरुरत से अब और इन्कार नहीं किया जा सकता। हमें एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है जो अलग-अलग शहरी समूहों को संसाधनों के साझे इस्तेमाल, शहरी योजना प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने और निर्णय लेने के अधिकार को स्थानीय स्तर तक ले जाने के विचारों पर काम करने के लिए एक साथ लाये।
बीजपत्र का यह संस्करण मुख्य रूप से शहर को सबके साझे की जगह बनाने और शहर में हो रही हिंसा के विरुद्ध इसकी भूमिका पर केन्द्रित रहेगा। ऐसा करने की कोशिश में, हम ऐसे नागरिकों और समुदायों के नजरिये को प्रमुखता देना चाहेंगे जो शहर की मौजूदा व्यवस्था (ऑर्डर) में निहित हिंसा से रोज रूबरू होते हैं। ख़ास तौर से भारतीय शहरी संदर्भ में इन प्रक्रियाओं और सम्बन्धों की समझ विकसित करना आज काफी जरुरी है। आज जब जलवायु संकट और सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी शहरी जीवन से जुड़ी आशाओं को ही खत्म कर दे रहे हैं, तो ऐसे समय में शहर को सबके साझे की जगह बनाने की कल्पना से शहर की प्लानिंग के मौजूदा तरीकों के मौलिक विकल्प निकल सकते हैं।
कॉमन्स या साझा संसाधन किसी भी रूप के हो सकते हैं, जैसे जल-जंगल-जमीन, ज्ञान, सांस्कृतिक धरोहर या इंटरनेट। एलेनोर ऑस्ट्रोम, जिन्होंने दुनिया भर के कई प्राकृतिक कॉमन्स का अध्ययन किया था, के अनुसार अगर राज्य या प्राइवेट कॉर्पोरेशनों का कब्जा नहीं रहे तो, जल निकायों, जंगलों और समुद्र में मछली पकड़ने के इलाके आदि जैसे कई सामाजिक-प्राकृतिक तंत्रों का समुचित और टिकाऊ प्रबंधन सामुदायिक रूप से किया जा सकता है। ‘कॉमन्स’ के साथ ही इससे जुड़ी एक और अवधारणा ‘कॉमनिंग’ भी महत्त्व की है। पीटर लिनबॉ ने कॉमनिंग को पारस्परिक सहायता (या एक दूसरे की देखभाल) पर आधारित एक सहकारी प्रक्रिया के रूप में समझाया है जिसके जरिये मिलजुलकर और जिम्मेदारीपूर्वक योजना बनाकर संसाधनों का इस्तेमाल हो। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह जमीन जहां से हमारा अनाज आता हे, ऊर्जा के स्रोत जिनसे हमारे शहर चलते हैं, और वह तकनीक जो हमारे जीवन को आसान बनाती है- इन सबका साझा इस्तेमाल और प्रबंधन किया जाना चाहिए और यही इस संस्करण का मुख्य सन्दर्भ बनाता है। इस चर्चा का सम्बन्ध राजनीतिक चेतना जगाने और हम पर असर डालने वाले हर मामले के निर्धारण में हमारा नियंत्रण वापस हासिल करने से भी है। यह सिर्फ एक काल्पनिक विचार नहीं है बल्कि समाज को व्यवस्थित करने का एक तरीका है जो दुनिया के कई हिस्सों में पहले से मौजूद है। इन तमाम प्रथाओं और ऐतिहासिक प्रयोगों से सीखकर, सामाजिक-पारिस्थितिक बदलाव की नई ताकत जुटाई जा सकती है और नागरिकों के तौर पर हमारी एक सामूहिक पहचान मजबूत की जा सकती है। सुनने में ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन सवाल ये है कि उपलब्ध साधनों के जरिये हम एकजुट होकर कैसे अपनी खोई हुई कल्पनाशक्ति को फिर से पाएं और एक अहिंसक, जीवित और मुक्त शहर को मुमकिन बनाएं।
हम इन सवालों के जवाब में सामाजिक कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं के योगदान आमंत्रित करते हैं। हम विशेष रूप से दलित, आदिवासी, महिलाओं और LGBTQIA+ समुदाय के योगदान आमंत्रित करते हैं। आप हमें अपने लेख, निबंध, कविता, कथा-कहानी (छोटे या बड़े दोनों प्रारूपों में), समीक्षा और कलाकृति (कैप्शन वाली तस्वीरें, कार्टून, कॉमिक्स और पोस्टर आदि) भेज सकते हैं। योगदान नीचे लिखे सवालों से जुड़े हो सकते हैं, या व्यापक तौर पर बीजपत्र के दायरे में आने वाले किसी भी विषय से जुड़े हो सकते हैं:
- राजसत्ता की हिंसा – विशेष रूप से पुलिस, नगर पालिकाओं और नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा, और इससे प्रभावित लोगों और समुदायों के अनुभव
- लैंगिक हिंसा – घरेलू स्थानों में, और सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों और सार्वजनिक परिवहन में; क्या बेहतर शहरी योजना के जरिये इसे रोका जा सकता है?
- दलितों और अन्य पीड़ित जातीय समुदायों के खिलाफ शहरों में जातिवाद और हिंसा; दलित आन्दोलन और जाति-विरोधी आंदोलन से उभरे विचार और उपाय
- वर्ग-आधारित हिंसा – आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, काम के बोझ का अत्याचार, शहर के अंदर और आसपास खेती की जमीनों का हड़पा जाना और खेतिहर समाज को बेदखल किया जाना, बेघर होना और किफायती दरों पर आवास की कमी, इत्यादि
- धार्मिक हिंसा – बढ़ती धार्मिक कट्टरता और सामाजिक ताने-बाने के टूटने के संदर्भ में
- बच्चों और युवा पीढ़ी के खिलाफ रोज़मर्रा की हिंसा – बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कों की कमी, खेलने के लिए उपयुक्त जगहों की कमी, स्कूल व्यवस्था के जरिये गलत शिक्षा दिया जाना, उम्र-आधारित ऊँच-नीच; और हिंसा के अन्य हालिया लेकिन प्रबल रूप जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली चिंताएँ
- परंपरागत ज्ञान के खो जाने या दुरुपयोग के रूप में हिंसा और असीमित शहरीकरण के विचार के कारण गाँव से मजबूरन शहर प्रवास और परंपरागत कौशल की हानि
- हिंसा के उपरोक्त रूप आपस में कैसे जुड़े हैं – इस पर चर्चा
- शहरी कॉमन्स/साझा शहर बनाने के विचारों से जुड़े अन्य पहलू जो शहर में किसी न किसी तरह की हिंसा को संबोधित करे; उदाहरण के लिए, शहरी खेती पर केंद्रित केस अध्ययन जो इसे खेती और खाद्य उत्पादन में बढ़ते कॉर्पोरेट नियन्त्रण के प्रतिरोध से जोड़ें
- शहर में या शहर की हिंसा से संबंधित कोई अन्य विषय
योगदान के लिए दिशानिर्देश
- नागरिक लेखकों, संगठनकर्ताओं, शोधकर्ताओं और कलाकारों के छोटे लेख, लंबे लेख, फिक्शन (लघु कथाएँ, कविताएँ, आदि), कैप्शन के साथ तस्वीरों, अन्य तरह के पोस्टर/चित्र का स्वागत है
- हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके योगदान आमंत्रित हैं
- छोटे लेख 1200 शब्दों से ज्यादा के न हों, और लंबे लेख 2000 शब्दों से ज्यादा के न हों। पत्रक में जगह की कमी के कारण बेहतर रहेगा कि आप छोटे लेख भेजने का प्रयास करें।
- चुने गए योगदानों को 1000-1500 रुपये का पुरस्कार (योगदान के प्रकार पर निर्भर) दिया जाएगा।
- कृपया अपना लेख या अन्य योगदान beejpatra@gmail.com पर 30 सितंबर, 2022 तक ईमेल करें
- युवा और नए लेखकों से विशेष अनुरोध है कि वे लेख आदि के विचार को पहले साझा करें ताकि हम शुरुआत से ही पत्रक में उनके योगदान को लेकर उनकी सहायता कर सकें।
- हम उन योगदानों को ही स्वीकार करेंगे जो अभी तक किसी भी रूप में (प्रिंट या ऑनलाइन) कहीं और प्रकाशित नहीं हुए हैं। हालाँकि, बीजपत्र एक “कॉपीलेफ्ट” प्रकाशन है, इसलिए बीजपत्र में प्रकाशित लेख आदि को उनके लेखक/लेखकों की अनुमति से कहीं और फिर से प्रकाशित किया जा सकता है।
*बीजपत्र जन संसाधन केंद्र, दिल्ली द्वारा पोषित है।